कुछ महीने पहले, जब मैं पर्यावरणीय मुद्दों पर लेख पढ़ रही थी, तो एक पंक्ति ने मुझे चौंका दिया: “हमारे पास केवल 60 फसलें बची हैं।” पहले तो यह सिर्फ एक और नाटकीय आँकड़ा लगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं और पढ़ती गयी, मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक शीर्षक नहीं था—बल्कि विज्ञान द्वारा समर्थित एक चेतावनी थी। यह चौंकाने वाला दावा मिट्टी के तेजी से हो रहे क्षरण की ओर इशारा करता है, न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि खासतौर पर भारत में, जहां कृषि आधी से अधिक आबादी की आजीविका का आधार है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अनुसार, भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 30% से अधिक अब “अपक्षीण” श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि मिट्टी ने अपनी प्राकृतिक उर्वरता और संरचना खो दी है—जो फसल उगाने, पानी को संरक्षित करने और जलवायु को नियंत्रित करने के लिए जरूरी गुण हैं। जब मैंने इस विषय पर और गहराई से शोध किया, तो स्पष्ट हो गया कि यह समस्या नई नहीं है, लेकिन यह हमारे पैरों के नीचे चुपचाप बढ़ती जा रही है, जबकि हमारा ध्यान अन्य अधिक स्पष्ट पर्यावरणीय मुद्दों पर है।
इस संकट के कारण मानवीय भी हैं और जलवायवीय भी। भारत में हरित क्रांति के दौरान कृषि में आए बदलावों ने फसल उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही ऐसी तकनीकें भी आईं, जिनसे मिट्टी की सेहत बिगड़ती चली गई। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और एक ही प्रकार की फसलों (मोनोकल्चर) पर निर्भरता ने मिट्टी से उसका जैविक पदार्थ और सूक्ष्मजीव जीवन छीन लिया। समय के साथ, गहरी जुताई, जैव विविधता का विनाश और अत्यधिक सिंचाई ने खेतों की बड़ी-बड़ी जमीनों को सूखा और बेजान बना दिया।
इसके ऊपर से, वनों की कटाई, शहरी विस्तार और औद्योगिक प्रदूषण ने कई क्षेत्रों की मिट्टी को पुनर्प्राप्ति से परे धकेल दिया है। ग्रामीण भारत में हमने बार-बार देखा है कि बाढ़ के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर ऊपरी परत की मिट्टी बह जाती है या सूखे के समय हवा में उड़ जाती है। यह केवल मिट्टी का नुकसान नहीं है—यह जीवन-समर्थन प्रणाली का नुकसान है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर साल लगभग 5.3 अरब टन मिट्टी खो देता है। यह मिट्टी कभी पूरी तरह से वापस नहीं आ सकती।
जो बात मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वह थी मिट्टी के स्वास्थ्य का जलवायु परिवर्तन से गहरा संबंध। स्वस्थ मिट्टी बड़ी मात्रा में कार्बन संचित करती है। जब मिट्टी खराब होती है, तो यह कार्बन वायुमंडल में छोड़ती है, जिससे वैश्विक तापवृद्धि और बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, मिट्टी केवल जलवायु परिवर्तन से पीड़ित नहीं है—अगर हम इसे नजरअंदाज करें, तो यह उसका कारण भी बन सकती है। यह विनाश का एक बंद चक्र है, जो खाद्य उत्पादन, जल सुरक्षा और अर्थव्यवस्था, सभी को प्रभावित करता है। खराब मिट्टी में उगाए गए खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे कुपोषण का खतरा बढ़ता है। साथ ही, ऐसी मिट्टी पानी को कम रोक पाती है, जिससे सूखे और बाढ़ की तीव्रता बढ़ जाती है।
हालांकि यह सब सुनने में बेहद चिंताजनक लगता है, लेकिन अब भी आशा बची है—अगर हम अभी कदम उठाएं।भारत के विभिन्न हिस्सों में कई समुदाय,स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय नेता इस क्षति को उलटने के लिए छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रयास कर रहे हैं।राजस्थान और तमिलनाडु जैसे स्थानों में किसान अब पुनरुत्पादक कृषि विधियों का उपयोग कर रहे हैं: कम्पोस्टिंग, फसल चक्र, आवरण फसल (मिट्टी को ढंकने के लिए लगाने वाली फसलें), और रासायनिक उत्पादों की जगह जैविक सामग्री का उपयोग। ये तकनीकें न केवल उपज बढ़ाती हैं, बल्कि मिट्टी की जैव विविधता और नमी को भी पुनर्स्थापित करती हैं।
भारत की पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ—जो टिकाऊपन के सिद्धांतों पर आधारित थीं—अब फिर से मान्यता प्राप्त कर रही हैं। गोबर और पत्तियों के अपशिष्ट से खाद बनाना, एक ही खेत में विभिन्न फसलें उगाना जैसी विधियाँ अब दोबारा अपनाई जा रही हैं लेकिन इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए व्यापक जन-जागरूकता और सरकारी समर्थन आवश्यक है।
हम क्या कर सकते हैं?
हमारे पास सबसे शक्तिशाली साधन है—जागरूकता। अधिकतर लोग, जैसा कि कभी मैं भी थी, मिट्टी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन जब यह समझ में आता है कि हम जो भी खाते, पहनते या उपयोग करते हैं, वह सब मिट्टी से शुरू होता है, तो सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सोशल मीडिया जैसे मंचों पर मिट्टी क्षरण की चर्चा एक व्यापक आंदोलन को जन्म दे सकती है। हर जागरूक आवाज, सतत भूमि उपयोग की मांग को और मजबूत करती है।
एक उपभोक्ता के रूप में, हम सचेत निर्णय ले सकते हैं—ऐसे स्थानीय किसानों से खरीदारी करें जो प्राकृतिक तरीकों से खेती करते हैं, टिकाऊता को प्राथमिकता देने वाले ब्रांडों को समर्थन दें, और भोजन की बर्बादी को कम करें। छोटे शहरों या फ्लैटों में भी रसोई के जैविक अपशिष्ट को खाद में बदला जा सकता है. इस सब प्रयासों का सीधा असर मिट्टी में जैविक तत्वों की वापसी कर पड़ता है।
हमें नीति-निर्माताओं पर भी दबाव डालना चाहिए। सरकारें मिट्टी के पक्ष में नीतियाँ बनाने, पुनरुत्पादक कृषि को प्रोत्साहित करने और भूमि पुनर्स्थापन परियोजनाओं में निवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। याचिकाओं पर हस्ताक्षर करना, सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेना या अपने प्रतिनिधियों को पत्र लिखना जैसे नागरिक प्रयास कृषि और पर्यावरणीय नीतियों में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।
सबसे जरूरी बात यह है कि हमें मिट्टी को देखने का नजरिया बदलना होगा—इसे निष्क्रिय या निर्जीव नहीं, बल्कि जीवंत और आवश्यक मानना होगा। मिट्टी हमारी सभ्यता की मौन नींव है। यह हमें भोजन देती है, हमारे पानी को छानती है, कार्बन संचित करती है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देती है। स्वस्थ मिट्टी के बिना कोई भी टिकाऊ भविष्य संभव नहीं है।
मेरे लिए जो यात्रा एक लेख से शुरू हुई, उसने जमीन को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। यह संकट असली है, और यहीं है। लेकिन समाधान भी यहीं हैं—विज्ञान, परंपरा और सामूहिक इच्छाशक्ति में निहित। मिट्टी को बचाना केवल प्रकृति को बचाने का कार्य नहीं है—यह उस आधार को सुरक्षित करने का कार्य है जिस पर हमारा समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन टिका है।
अब समय आ गया है कदम उठाने का—क्योंकि एक बार मिट्टी चली गई, तो वह फिर नहीं लौटेगी।



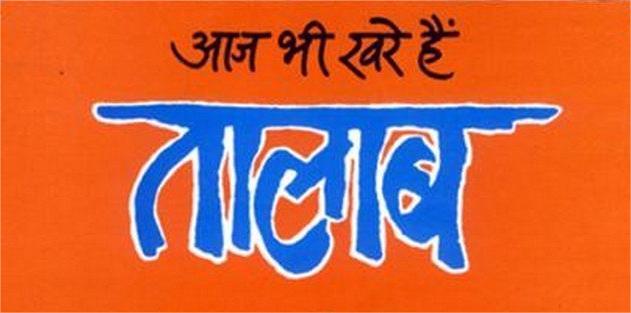

Leave a Reply