बहुत समय पहले की बात है, आर्कटिक की बर्फीली बाहों में ‘नानूक’ नाम का एक ध्रुवीय भालू रहता था। उसका नाम, जिसका अर्थ है “महान शिकारी”, उसे उसके पूर्वजों ने दिया था—वे पूर्वज जो उस दुनिया में फले-फूले जहाँ बर्फ गहरी थी, मछलियाँ प्रचुर मात्रा में थीं, और दुनिया संतुलन में थी। लेकिन वह दुनिया अब बदल रही थी—इतनी तेजी से कि नानूक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
नानूक का जन्म स्वालबार्ड द्वीपसमूह की कड़ाके की ठंडी बर्फ पर हुआ था। उसकी माँ, ‘अम्का’, ने उसे बर्फीले पानी में तैरना और बहती बर्फ पर सील का पीछा करना सिखाया था। लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते गए, नानूक के शिकार क्षेत्र सिकुड़ते गए। जो बर्फ एक समय क्षितिज तक फैली होती थी, अब मौसम की शुरुआत में ही टूटने लगी थी। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी, “जब बर्फ पिघलती है, तो सील गायब हो जाती हैं, और हमें लंबी दूरी तक तैरना पड़ता है, नानूक। लेकिन समुद्र हमेशा दयालु नहीं होता।”
नानूक का संसार उसके पंजों के नीचे पिघल रहा था। वह पूरी ताकत से तैरता रहा, लेकिन सामने बस बिखरती बर्फ और भूख की आशंका थी।
हज़ारों मील दूर एशिया में भी एक और मौन संकट जन्म ले रहा था।
हिमालय और हिंदूकुश की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं वाला एशिया अपने ग्लेशियरों को चिंताजनक गति से खो रहा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) के अनुसार, हिमालयी ग्लेशियरों ने पिछले कुछ दशकों में लगभग 40% क्षेत्रफल खो दिया है। यदि यही रुझान जारी रहे, तो इस सदी के अंत तक क्षेत्र के दो-तिहाई ग्लेशियर समाप्त हो सकते हैं।
एशिया के लिए, ग्लेशियर केवल बर्फीले पहाड़ नहीं हैं—ये 1.9 अरब लोगों के जीवन का आधार हैं, जो इनसे निकलने वाली नदियों पर निर्भर हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांग्त्से जैसी नदियाँ—जो इन ग्लेशियरों की बर्फ से पोषित होती हैं—अब मौसमी धाराओं में बदलने की कगार पर हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति और आजीविका को खतरा है।
विश्व जल दिवस की झलक: ग्लेशियरों से जुड़ा हमारा भविष्य
पिछले सप्ताह, हमने 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस पर ग्लेशियरों के महत्व पर विचार किया। इस वर्ष की थीम थी “सतत भविष्य के लिए ग्लेशियरों का संरक्षण”। हमने 1992 के पृथ्वी सम्मेलन (UNCED) की चर्चा की, जिसने एजेंडा 21 और रियो घोषणा के माध्यम से वैश्विक प्राथमिकताओं की नींव रखी। इन पहलों ने समय के साथ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को आकार दिया है। इस वर्ष, इस दिन ने चेताया कि यदि हम ग्लेशियरों को नहीं बचाते, तो एशिया की जल सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
जलवायु प्रभाव: जब नानूक और एशिया टकराते हैं
भले ही नानूक का घर और एशिया के ग्लेशियर हज़ारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन इन दोनों का संकट एक जैसी त्रासदी को दर्शाता है। अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जन से बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ध्रुवीय और पर्वतीय ग्लेशियर समान रूप से पिघल रहे हैं।
IPCC की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, यदि तापमान में वृद्धि ऐसे ही जारी रही, तो 2050 तक आर्कटिक समुद्री बर्फ गर्मियों में पूरी तरह गायब हो सकती है। हिंदूकुश हिमालय मूल्यांकन रिपोर्ट भी चेताती है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित कर भी दिया जाए, तब भी क्षेत्र के ग्लेशियर 2100 तक 36% तक सिकुड़ सकते हैं।
सिर्फ जागरूकता नहीं, अब ज़रूरत है कार्रवाई की
नानूक की लड़ाई उन अरबों लोगों की कहानी है जो ग्लेशियरों के पानी पर निर्भर हैं। हर वर्ष, जैसे-जैसे उसके पैरों तले की बर्फ पतली होती जाती है, उसका जीवित रहने का मौका कम होता जाता है। एशिया में किसान, जो इन नदियों से सिंचाई करते हैं, अब बंजर खेतों को देख रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी बढ़ रही है, और जैव विविधता अस्थिर बहाव से प्रभावित हो रही है।
लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है। हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं।
हम क्या कर सकते हैं?
- अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें: सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, एयर ट्रैवल कम करें, ऊर्जा-कुशल उपकरण अपनाएं, स्थानीय और टिकाऊ उत्पादों को प्राथमिकता दें।
- जल संरक्षण और कचरे में कमी लाएँ: घर पर पानी बचाएं, लीक ठीक करें, वर्षा जल संग्रह करें, और प्लास्टिक का उपयोग घटाएं।
- स्थानीय प्रयासों का समर्थन करें: पर्यायवरण, जल और ग्लेशियर संरक्षण के लिए किये जा रहे सरकारी, गैर सरकारी और व्यक्तिगत प्रयासों के बारे में जानकारी बढायें एवं उनसे जुडें।
- पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा दें: मंगोलिया के घुमंतू चरवाहे या नेपाल के पहाड़ी समुदाय, सदियों से ग्लेशियरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते आ रहे हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान को समझें और उसका सम्मान करें।
अब चुनाव हमारा है—बदलाव लाना है या मौन पुकार को अनसुना करना है।
मौन पुकार: क्या हम सुनेंगे?
जब नानूक पिघलती बर्फ पर स्थिर जमीन खोजने की कोशिश करता है, वह सोचता है—क्या दुनिया सुन रही है? उसके पूर्वजों ने एक ऐसे संसार में जीवन जिया जहाँ ग्लेशियर अमर थे, लेकिन अब वे सिर्फ यादें बनते जा रहे हैं। हिमालय में भी, हजारों वर्षों से जीवन देने वाली नदियाँ अब पिघलती बर्फ की सरसराहट बनकर रह गई हैं।
क्या हम इन मौन पुकारों को सुनेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए?
आशा की किरण: नानूक की अंतिम गुहार
नानूक की यात्रा समाप्त नहीं हुई है। वह सिकुड़ते हिमखंडों के साथ बहता जा रहा है, एक आशा के साथ—कि दुनिया जागेगी, नेता अपने टिकाऊ विकास के वादों को निभाएंगे, और अगली पीढ़ियाँ एक ऐसी पृथ्वी की वारिस बनेंगी जहाँ ग्लेशियर जीवन के प्रहरी हों, न कि विलुप्त स्मृतियाँ।
लेकिन सिर्फ आशा काफी नहीं है। अब वक्त है—आशा से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने का। इससे पहले कि नानूक और एशिया के ग्लेशियरों की पुकार इतिहास बन जाए।


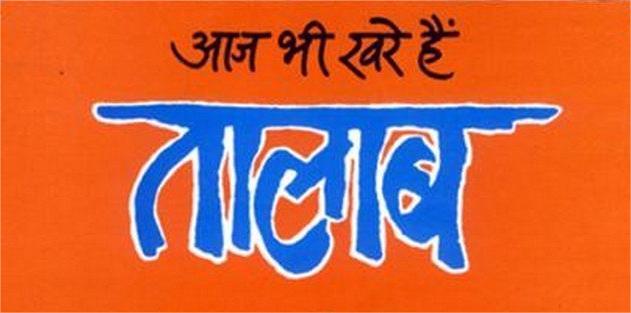

Leave a Reply